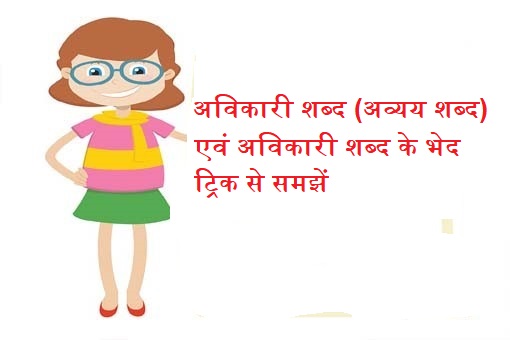अविकारी शब्द किसे कहते हैं?
वाक्य मे प्रयोग किये जाने वाले जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं।
अर्थात वे शब्द जिन्हे लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला न जा सके, अविकारी शब्द कहलाते हैं।
जैसे – अब, कब, क्यों, पर, में, बहुत, अधिक, कम, हाँ, नहीं, लेकिन, जल्दी, शीघ्र आदि।
अविकारी शब्द के भेद
अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं –
- क्रिया-विशेषण
- संबंधबोधक
- समुच्चयबोधक
- विस्मयबोधक
क्रिया-विशेषण किसे कहते हैं?
वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया-विशेषण कहलाते हैं।
जैसे – राम चलता है।
उपरोक्त वाक्य में ‘राम’ कर्ता तथा ‘चलता’ क्रिया है। यदि मैं कहूँ कि –
राम धीरे / तेज चलता है।
तो उपरोक्त वाक्य में धीरे / तेज क्रिया-विशेषण होगा।
अन्य उदाहरण –
- हिरण तेज चलता है।
- रवि ऊपर बैठा है।
- संदीप नीचे खड़ा है।
उपरोक्त वाक्य में तेज, ऊपर, नीचे शब्द क्रिया की विशेषता बताते है अतः ये शब्द क्रिया-विशेषण हैं।
क्रिया-विशेषण अव्यय क्रिया से ठीक पहले आता है।
क्रिया – विशेषण के महत्व / आवश्यकता
क्रिया-विशेषण के निम्नलिखित महत्व / आवश्यकता हैं –
एक क्रिया-विशेषण दूसरे क्रिया-विशेषण की विशेषता बताता है|
जैसे – बहुत चालाक बालक बहुत तेज बोलते हैं।
बहुत – प्रविशेषण
चालाक – गुणवाचक विशेषण
बालक – कर्ता
बहुत तेज – क्रिया विशेषण
बोलते – क्रिया
क्रिया-विशेषण क्रिया की स्वीकृति बताते हैं।
जैसे – हाँ जाओ।
हाँ – क्रिया विशेषण (क्योकि स्वीकृति बताते हैं)
जाओ – क्रिया
मत जाओ|
यहाँ ‘मत’ शब्द निषेधता को बताते हैं इसलिए ‘मत’ शब्द क्रिया-विशेषण नहीं होगा।
क्रिया-विशेषण क्रिया की निश्चितता बताते हैं।
जैसे – आज बारिस जरूर आयेगी।
यहाँ ‘जरूर’ शब्द निश्चितता को प्रकट कर रहे हैं।
क्रिया-विशेषण क्रिया की अनिश्चितता भी बताते हैं।
जैसे – आज वर्षा शायद आयेगी।
यहाँ ‘शायद’ शब्द अनिश्चितता को प्रकट कर रहे हैं।
क्रिया-विशेषण से क्रिया के होने का समय भी पता चलता है।
जैसे – श्याम दो घण्टे पढ़ता है|
क्रिया-विशेषण क्रिया के होने का स्थान भी बताते हैं।
जैसे – श्याम छत पर खड़ा है।
क्रिया-विशेषण क्रिया के होने की दिशा भी बताते हैं।
जैसे – सूर्योदय पूर्व में होता है।
क्रिया-विशेषण संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है।
जैसे – इधर देखो।
मेरी ओर देखो।
क्रिया-विशेषण क्रिया के होने की मात्रा बताते हैं।
जैसे – श्याम खूब सोता है, कम पढ़ता है|
श्याम – कर्ता
खूब – मात्रा
सोता – क्रिया
कम – मात्रा
पढ़ता – क्रिया
क्रिया-विशेषण के प्रकार
क्रिया-विशेषण चार प्रकार के होते हैं जो नीचे दिये गए हैं –
- कालवाचक क्रिया-विशेषण
- स्थानवाचक क्रिया-विशेषण
- परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण
- रीतिवाचक क्रिया-विशेषण
कालवाचक क्रिया-विशेषण किसे कहते हैं ?
क्रिया के होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषणों को कालवाचक क्रिया-विशेषण कहा जाता है।
जैसे – पक्ष, बजे का समय या अवधि, आज, कल, सप्ताह, वर्ष, माह, वार आदि।
उदाहरण – राम आज आयेगा।
स्थानवाचक क्रिया-विशेषण किसे कहते हैं ?
क्रिया के होने का स्थान, दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया-विशेषण कहलाता है।
जैसे – श्याम छत पर बैठा है।
श्याम – कर्ता
छत – क्रिया-विशेषण
पर – विभक्ति
छत पर – स्थानवाचक
(स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही अधिकरण कारक होता है।)
परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण किसे कहते हैं ?
क्रिया के होने की मात्रा बताने वाले क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण होते है।
जैसे – श्याम बहुत सोता है।
राधा कम पढ़ती है।
जितनी गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा।
रीतिवाचक क्रिया-विशेषण किसे कहते हैं ?
क्रिया के होने का ढंग / तरीका बताने वाले शब्दों को रीतिवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं।
इसमे क्रिया की स्वीकृति, निषेधता, निश्चितता व अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द भी शामिल किये जाते हैं।
जैसे – श्याम सरपट दौड़ता है।
यहाँ ‘सरपट’ शब्द रीतिवाचक क्रिया-विशेषण है।
संबंधबोधक अव्यय किसे कहते हैं?
जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ता है, वह संबंधबोधक कहलाता है।
अर्थात संबंध का बोध कराने वाले अव्यय पद को संबंधबोधक अव्यय कहलाते हैं।
जैसे – के बिना, दूर, निकट, ऊपर, नीचे, बीच, सामने, आगे, पीछे, दाएँ, बाएँ, खिलाफ, बिना, अंदर, ओर, साथ, सहित, पास, आस – पास, बिना, बगैर, हेतु, लिए, कारण आदि।
उदाहरण – राधा के बिना श्याम परेशान हैं।
उपरोक्त वाक्य में ‘के बिना’ शब्द संबंधबोधक अव्यय है।
संबंधबोधक अव्यय एक ही वाक्य में दो पदो के मध्य पाये जाते हैं।
समुच्च्य बोधक अव्यय किसे कहते हैं?
समूह (समुच्च्य) का बोध कराने वाले अव्यय पद समुच्च्य बोधक अव्यय कहलाते हैं।
जैसे – लेकिन, तथा, किन्तु, परन्तु, और, या, अथवा, एवम्, जो, जिसे, जिन्हें, जैसे – जैसे, बल्कि आदि।
उदाहरण – श्याम पढ़ता है लेकिन राम सोता है, तथा राधा भोजन बना रही है।
श्याम पढ़ता है – उपवाक्य
राम सोता है – उपवाक्य
भोजन बना रही है। – उपवाक्य
लेकिन – समुच्च्य बोधक अव्यय
तथा – समुच्च्य बोधक अव्यय
अर्थात उपवाक्यो को जोड़ने वाले शब्दों या पदों को समुच्च्य बोधक अव्यय कहते हैं।
समुच्च्य बोधक अव्यय दो उपवाक्यो के मध्य पाये जाते हैं।
समुच्च्य बोधक अव्यय के प्रकार
समुच्च्य बोधक अव्यय निम्न प्रकार के होते हैं –
- समानाधिकरण (संयुक्त वाक्य)
- व्याधिकरण (मिश्र वाक्य)
विस्मयादिबोधक अव्यय किसे कहते हैं?
आश्चर्य / अचरज आदि का बोध कराने वाले अव्यय को विस्मयबोधक अव्यय कहते हैं।
जैसे – अरे, अहो, अजी, उफ, धत्, धतेरेकी, हफ, शाबाश, अरे वाह, अजी सुनते हो, धन्यवाद आदि।
उदाहरण – वाह ! कितना सुन्दर नजारा है। विस्मयादिबोधक अव्यय वाक्यो के आरम्भ मे होते हैं।
हिन्दी व्याकरण ..