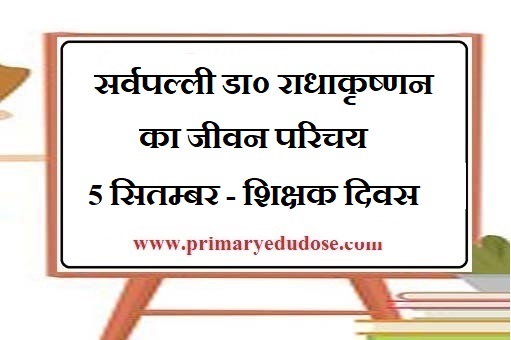| जन्म | 5 सितम्बर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी गाँव में |
| पिता का नाम | सर्वपल्ली वीरास्वामी |
| माता का नाम | श्रीमती सीतम्मा |
| मृत्यु | 17 अप्रैल, 1975 |
| उपलब्धि | भारत रत्न |
5 सितम्बर का दिन महान दार्शनिक, कुशल शिक्षक एवं गणतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णन की याद दिलाता है।
इनका जन्म 5 सितम्बर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी गाँव में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती सीतम्मा तथा पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था।
इनकी आरम्भिक शिक्षा गाँव के ही स्कूल में हुई। तत्पश्चात मद्रास (चेन्नई) क्रिश्चियन कॉलेज से बी०ए० एवं एम०ए० की परीक्षा पास की। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विवाह 17 वर्ष की उम्र में ही शिवकमुअम्मा से हो गया।
मद्रास प्रेसिडेन्सी कॉलेज के सहायक अध्यापक पद से शुरू करके विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति तक के सफ़र में इन्होंने कई महत्त्वपूर्ण कार्य किये। ये जहाँ भी गये वहाँ कुछ न कुछ सुधारात्मक बदलाव जरुर हुआ। आन्ध्र विश्वविद्यालय की इन्होंने आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय को राजधानी का श्रेष्ठ ज्ञान केन्द्र बनाने का भरपूर प्रयास किया।
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए किया गया इनका कार्य विशेष उल्लेखनीय है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारत छोड़ो आन्दोलन में बढ़कर हिस्सा लिया। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के तात्कालिक गवर्नर सर हेलेट ने क्रुद्ध होकर विश्वविद्यालय को युद्ध अस्पताल में बदल देने की धमकी दी।
डा० राधाकृष्णन तुरन्त दिल्ली गये और वहाँ वायसराय लार्ड लिनालियगो से मिले। उन्हें अपनी बातों से प्रभावित कर गवर्नर के निर्णय को स्थगित कराया। फिर एक नई समस्या आई। क्रुद्ध गवर्नर ने विश्वविद्यालय की आर्थिक सहायता बंद कर दी। लेकिन राधाकृष्णन ने शांतिपूर्वक येनकेन प्रकारेण धन की व्यवस्था की और विश्वविद्यालय संचालन में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया।
सन् 1949 ई० में राधाकृष्णन को सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में चुना गया। सन् 1955 ई० में ये भारत के उप राष्ट्रपति के पद पर चुने गये। तथा सन् 1962 ई० में ये भारतीय गणतंत्र के दूसरे राष्ट्रपति बने। इनके राष्ट्रपति पद से मुक्ति होने के बाद मई 1967 में मद्रास स्थित अपने घर के सुपरिचित माहौल में लौट आये और जीवन के अगले आठ वर्ष बड़े ही आनंदपूर्वक व्यतीत किये।
भारतीय दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान, कुशल राजनीतिज्ञ एवं अद्विवतीय शिक्षक के रूप में विख्यात डा० राधाकृष्णन 17 अप्रैल, 1975 को इस दुनिया से चल बसे।
प्रमुख पुस्तकें
- द एथिक्स आफ वेदान्त
- द फिलासफी आफ रवीन्द्र नाथ टैगोर
- माई सर्च फार टुथ
- द रेन आफ कंटम्परेरी फिलासफी
- रिलीजन एण्ड सोसाइटी
- इण्डियन फिलासफी
- द एसेन्सियल आफ सायकालजी
उपलब्धि
शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार की ओर से वर्ष 1954 ई० में इन्हें स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च सम्मान ‘भारत रत्न’ से विभूषित किया गया। ये ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे। वास्तव में उनका भारत रत्न से सम्मानित किया होना देश के हर शिक्षक के लिए गौरव की बात है।
राजनीतिक क्षेत्र में कार्य
सन् 1949 ई० राधाकृष्णन को सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में चुना गया। उस समय वहां के राष्ट्रपति थे जोसेफ स्तालिन। इनके चयन से लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आदर्शवादी दर्शन की व्याख्या करने वाला एक शिक्षक भला भौतिकवाद की धरती पर कैसे टिक पायेगा?
लेकिन सबको विस्मृत करते हुए इन्होंने अपने चयन को सही साबित कर दिखाया। इन्होंने भारत और सोवियत रूस के बीच सफलतापूर्वक एक मित्रतापूर्वक समझदारी की नीव डाली। इन्हें विदेशों में जब भी मौका मिलता स्वतंत्रता के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने से नहीं चूकते।
शासनाध्यक्ष राधाकृष्णन
सन् 1955 में राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के उप राष्ट्रपति के पद पर चुने गये। यह चुनाव आदर्श साबित हुआ। जितनी मर्यादा उन्हें उपराष्ट्रपति पद से मिली उससे कहीं ज्यादा उन्होंने उस पद की मर्यादा में वृद्धि की। सन् 1962 ई० ये भारतीय गणतंत्र के दूसरे राष्ट्रपति बने। वे कभी भी एक दल अथवा कार्यक्रम के समर्थक नहीं रहे।
सरस वक्ता
डा० राधाकृष्णन एक कुशल वक्ता थे। इनके वक्तव्य को लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। वे गंभीर से गंभीर विषयों का प्रस्तुतीकरण अत्यन्त सहज रूप से कर लेते थे। मद्रास प्रेसिडेंसी कालेज के एक छात्र के शब्दों में-
”जितनी देर तक वे पढ़ाते थे, उतने समय तक उनका प्रस्तुतीकरण उत्कृष्ट था। वे जो भी पढ़ाते थे, सभी के लिए सुगम था।”
डा० राधाकृष्णन के विचार
1. धर्म का लक्ष्य अंतिम सत्य का अनुभव है।
2. दर्शन का उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना नहीं, जीवन को
बदलना है।
3. रोटी के ब्रह्म को पहचानने के बाद, ज्ञान के ब्रह्म से साक्षात्कार
अधिक सरल हो जाता है।
4. दर्शन का जन्म सत्यानुभव के फलस्वरूप होता है न की खोजों
के इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप।
5. दर्शनशास्त्र एक रचनात्मक विद्या है।
6. अंतरात्मा का ज्ञान नष्ट नहीं होता है।
7. प्रत्येक व्यक्ति ही ईश्वर की प्रतिमा है।
8. एक शताब्दी का दर्शन ही, दूसरी शताब्दी का सामान्य ज्ञान होता
है।