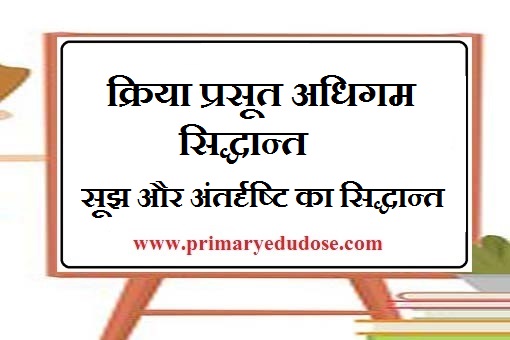इस सिद्धान्त का प्रतिपादन स्किनर महोदय के द्वारा किया गया है। इन्होने पावलव के अनुबंध सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा है कि प्राणी व्यवहार करने के लिए उद्दीपक की प्रतीक्षा नहीं करता है और न ही वह यंत्रवत प्रतिक्रिया करता है। बल्कि उसके व्यवहार का अनुबंध परिणाम पर आश्रित होता है। यदि परिणाम संतुष्टदायक होता है। तो प्राणी दुबारा प्रतिक्रिया करता है। अर्थात वह क्रिया करने के लिए स्वतंत्र होता है।
यह परिणाम अर्थात पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं –
- धनात्मक पुनर्वलन
- ऋणात्मक पुनर्वलन
धनात्मक पुनर्वलन मे वांछित क्रिया बार – बार दोहराने के लिए दिया जाता है।
जैसे – प्रशंसा, पुरस्कार आदि।
ऋणात्मक पुनर्वलनमे पुनर्वलन को हटाकर वांछिक क्रिया के बार – बार करने की संभावनाओ मे वृद्धि की जाती है।
जैसे – शोर, निंदा आदि।
यह पुनर्वलन प्राणी को दो रूपों मे दिया जाता है –
- सतत
- असतत
सतत पुनर्वलन प्राणी की प्रत्येक अनुक्रिया पर दिया जाता है। जबकि असतत पुनर्वलन मे निरंतरता का अभाव होता है।
असतत पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं –
- अनुपातिक
- अंतराल
आनुपातिक पुनर्वलनमे एक निश्चित क्रम मे पुनर्वलन दिया जाता जबकि अंतराल पुनर्वलन समय आधारित होता है और एक निश्चित समय पर दिया जाता है।
क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धान्त का प्रयोग
इस सिद्धान्त का प्रयोग स्किनर महोदय ने चूहो पर किया। इस सिद्धान्त मे स्किनर महोदय ने चूहों पर अनेक प्रयोग किए। उसने एक बाक्स बनवाया जिसमे एक लीवर लगा था। लिवर पर चूहे का पैर पड़ते ही खट की आवाज होती, आवाज को सुनकर चूहा आगे बढ़ता और प्याले मे रखें भोजन को प्राप्त कर लेता। भोजन चूहे के लिए प्रवलन का कार्य करता था। चूहा भूखा होने पर प्रणोदित होता और लीवर को दबाता तथा भोजन प्राप्त कर लेता।
इस प्रयोग के बाद स्किनर महोदय ने निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति मे बृद्धि हो जाती है।
क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धान्त का शिक्षा मे महत्व
- इस सिद्धान्त के द्वारा सीखने मे गति तथा सरलता प्रदान होती है।
- इस सिद्धान्त के द्वारा बालको की समायोजन क्षमता का विकास होता है।
- इस सिद्धान्त द्वारा अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है।
- यह सिद्धान्त मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार के सीखने मे विशेष रूप मे सहायक हुआ है।
सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धान्त (sujh ka siddhant)
सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धान्त के प्रतिपादक का नाम कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर और कूर्ट्लेविन है।
इन्होने मनोविज्ञान मे गेस्टाल्टवाद का प्रतिपादन किया। गेस्टाल्टवाद जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ संगठित या पूर्ण आकृति से है। इनका मानना है कि व्यक्ति का सीखना अभ्यास एवं प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। बल्कि वह परिस्थितियों का पूर्ण अवलोकन या संबंध पर आधारित होता है। जिसे सूझ कहते हैं। यह सूझ अचानक, स्वतः स्फूर्ति पर आधारित होता है।
इनका मानना है कि प्राणी के सम्मुख जब कोई समस्या आती है तब प्राणी उस परिस्थिति मे उपस्थित तत्वो मे संबंध स्थापित करता है। इसी संबंध मे उसे अचानक सूझ प्राप्त होती है और वह समस्या का समाधान कर लेता है इसी को अधिगम कहते हैं।
सूझ सिद्धान्त का प्रयोग
इस सिद्धान्त मे कोहलर ने वनमानुषो पर प्रयोग किया। उन्होने वनमानुषो को एक कमरे मे बंद कर दिया और कमरे की छत मे एक केला लटका दिया और कुछ दूर पर एक बाक्स भी रख दिया। वनमानुषो ने केले को प्राप्त करने के लिए खूब उछल कूद किया लेकिन असफल रहे। उन सभी वनमानुषो मे एक सुल्तान नाम का वनमानुष था उसने कमरे मे इधर – उधर घूमा और बाक्स के पास जाकर खड़ा हुआ। सुल्तान नामक वनमानुष ने उस बाक्स को खींचा और केले के नीचे ले गया और बाक्स के ऊपर चड़कर केला प्राप्त किया।
अतः सुल्तान के इस कार्य से सिद्ध होता है कि उसमे सूझ थी, जिसने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने मे सफलता प्राप्त की।
सूझ सिद्धान्त का शिक्षा मे महत्व
- यह सिद्धान्त रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है।
- इस सिद्धान्त के द्वारा बालकों की बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास होता है।
- यह सिद्धान्त गणित जैसी विषयो के शिक्षण के लिए लाभप्रद है।
सम्पूर्ण—–bal vikas and pedagogy—–पढ़ें
इसे भी पढ़ें –
वायु, जल, ध्वनि और मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं ?